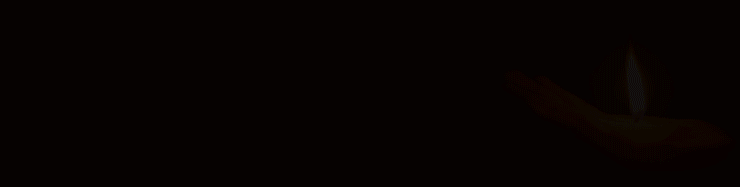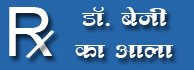मैं यह नहीं कतई नहीं कह रहा कि पा फिल्म बेकार है। पा फिल्म तो वाकई तारीफ पाने की हकदार है। पर इसलिए नहीं कि वह प्रोजेरिया से पीड़ित एक बच्चे की कहानी है, या इसलिए भी नहीं कि प्रोजेरिया से पीड़ित १२ साल के बच्चे औरो की भूमिका में बिग बी ने 'कमाल' कर दिया है। इसलिए तो कतई नहीं कि जूनियर बी ने बिग बी के पिता का रोल किया।
तारीफ इसलिए होनी चाहिए
- कि इंटरनैशनल मेकअप आर्टिस्ट कर्स्टन टिंबल और डोमिनिक ने अपने कौशल से अमिताभ बच्चन को बिग बी के करेक्टर से बाहर कर दिया है। यह एक बड़ी वजह है कि औरो की भूमिका में दर्शकों को अपने अमिताभ का चेहरा नहीं दिखता। रही सही कसर खुद बिग बी ने पूरी कर दी अपनी वाइस मॉड्यूलेशन से।
- कि ऐड एजेंसी के क्रिएटिव हेड रहे बाल कृष्णन (बाल्की) चूक गये। वह चाहते तो स्क्रिप्ट की डिमांड के तर्क के साथ विद्या बालन और अभिषेक के अंतरंग क्षणों की शूटिंग कर सकते थे। फिल्म के प्रोमो में इन दृश्यों को ठूंस कर दर्शकों का बड़ा हुजूम खींच सकते थे।
- कि बाल्की ने वाकई पा को भुनाने के लिए किसी सस्ते हथकंडे का इस्तेमाल न कर अपनी क्रिएटिविटी पर भरोसा किया।
- कि यह फिल्म सिर्फ औरो की कहानी नहीं है। यह विद्या के संघर्ष की कहानी है। अमोल आम्टे की महत्वाकांक्षा की भी कहानी है। मीडिया की नासमझी-नादानी की भी दास्तां है। तिसपर चारों कहानियां एक साथ चल रही हैं और ऊबने नहीं देतीं। स्क्रिप्ट की बुनावट इतनी सधी और कसी हुई कि इन कहानियों को आप एक-दूसरे से अलग नहीं कर सकते।
- कि निर्देशकीय पकड़ इतनी सख्त है कि फिल्म के करेक्टरों की तमाम मासूमियत आपके साथ चलने लगती है। आप उस अमोल आम्टे के लिए आक्रोश भी नहीं पाल पाते, जिसकी वजह से पैदा हुए तनाव का असर एक बच्चे की जिंदगी पर पड़ता है। यह असर इतना भयंकर है कि बच्चा पैदा हुआ तो अपने को प्रोजेरिया से घिरा पाया। फिल्म हॉल से निकलते ही औरो आपके जेहन में घूम रहा होता है, शेष करेक्टर महज औरो को बुन रहे होते हैं।
नहीं है इसमें बिग बी का चमत्कारिक अभिनय

कुछ फिल्में अपनी शानदार तकनीक की वजह से याद की जाती हैं, तो कुछ शानदार एक्टिंग की वजह से। किसी में स्क्रिप्ट जानदार होती है तो किसी में निर्देशन शानदार। तकनीकों का कमाल अब की हिंदी फिल्मों में दिखने लगा है। गाहे-बगाहे लीक से हटकर किया गया मेकअप भी पब्लिक का ध्यान खींचता रहा है। पर पा में जिस करेक्टर के इर्द-गिर्द पूरी फिल्म घूमती है वह है औरो। इस औरो का मेकअप इतना सटीक है कि दर्शक उसके करेक्टर की खासियतों से बगैर संवाद जुड़ जाता है। किसी करेक्टर को जीवंत बनाने में एक्टिंग का बड़ा योगदान होता है। एक्टिंग के तीन खास पक्ष होते हैं - फेशिअल एक्स्प्रेशन, बॉडी लैंग्वेज और वाइस मोड्यूलेशन। फिल्म की बाकी तमाम चीजें एक्टिंग के इन तीन खास पॉइंट्स का साथ देती हैं। पा में औरो का मेकअप ऐसा है कि फेशियल एक्सप्रेशन की गुंजाइश किसी आर्टिस्ट के लिए बच नहीं पाती। रही बात बॉडी लैंग्वेज की, तो जाहिर है वह अपंग बच्चे जैसी ही होगी। यह काम किसी भी प्रफेशनल आर्टिस्ट के लिए जरा भी मुश्किल नहीं। हां, वाइस मॉड्यूलेशन में सामान्य सी गुंजाइश थी जिसे बिग बी ने आसानी से पूरा किया।
तो फिर ऐसी सामान्य-सी एक्टिंग के लिए बिग बी का ही सिलेक्शन क्यों हुआ? और हुआ भी तो बिग बी जैसे आर्टिस्ट ने इसे स्वीकार क्यों कर लिया?
दरअसल, बाल्की ऐड एजेंसी के हेड रहे हैं। उन्हें खूब पता है कि किसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए ऐड कैसा होना चाहिए। पा जैसे प्रोडक्ट (जो लीक से हटकर है) का बाजार बनाना आसान नहीं था। इसे चर्चा में लाने के लिए बिग बी से बड़ा नाम दूसरा हो नहीं सकता था। विज्ञापन की आंखों ने यह भी देखा कि बिग बी की उम्र 70 के आसपास है और पा के औरो की 12 के आसपास। तो उम्र के इस कंट्रास्ट को भुनाया जा सकता है। प्रोडक्ट के बिकने के रास्ते में जो थोड़ी बहुत हिचक रही होगी उसे उन्होंने जूनियर बी को जोड़ कर दूर कर लिया। क्योंकि अब बाल्की के पास प्रचार के लिए करेक्टर और कलाकार का कंट्रास्ट तो था ही, बिग बी (बेटा) और जूनियर बी (बाप) के रोल की केमेस्ट्री भी थी। विज्ञापन की आंखों ने वाकई अपना असर दिखाया।
हर कलाकार की चाहत होती है कि वह खुद को डिफरेंट रंगों में देखे। औरो के असामान्य रंग में खुद को देखने की ख्वाहिश बिग बी की भी रही होगी - यह समझा जाये, तो यह समझ दोषपूर्ण नहीं। हां, यह जरूर है कि इसके अलावा भी कुछ कारण रहे होंगे जिन्होंने बिग बी को बाध्य किया होगा इस रोल को स्वीकार करने में।
विद्या का प्रेम, आम्टे का पलायन
पा में विद्या मेडिकल स्टूडेंट है। जीवन के किसी मोड़ पर उसकी मुलाकात अमोल आम्टे नाम के नौजवान से हो जाती है। बढ़ते भरोसे के साथ दोनों की मुलाकातें भी बढ़ती हैं। मुलाकातों के बढ़े अंतरंग कदम का पता उन्हें तब चलता है जब उनके सामने सिर्फ दो ही रास्ते बचते हैं - या तो शादी या अबॉर्शन।
आम्टे बेहद महत्वाकांक्षी करेक्टर है। भरोसे से लबरेज। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण उसका करियर है। इस करियर के रास्ते में किसी भी 'लिजलिजी संवेदना' के लिए कोई जगह नहीं। ऐसे हर बैरियर को कुचलते और लताड़ते हुए उसे आगे बढ़ना है। एक बड़ा और जिम्मेवार नेता बन कर देश का भविष्य संवारना है। यही सीख वह विद्या को भी देता है। उसे याद दिलाता है कि अगर बच्चे-वच्चे के फेर में वह पड़ी तो उसके डॉक्टर बनने का ख्वाब अधूरा रह सकता है। बेहतर होगा अबॉर्शन करा ले।
दो स्त्रियों का हौसला
विद्या मजबूत इच्छाशक्ति वाली करेक्टर है। जो किया, उसपर कोई पश्चाताप नहीं। जो आएगा उसका सामना करना, उससे जूझना, उसे जीना विद्या को ज्यादा पसंद है। विद्या की मजबूती के पीछे उसकी मां का भी हौसला है, जो - हे भगवान, तूने ये क्या किया - जैसे किसी संवाद से कोसने की बजाए विद्या से पूछती हैं कि तुम्हें बच्चा चाहिए या नहीं? जब विद्या बच्चे को जन्म देने की अपनी इच्छा जताती है तो मां उसे गले लगा लेती हैं। वह घर और बच्चे की पूरी जिम्मेवारी इस कदर ओढ़ लेती हैं कि विद्या का करियर न डगमगाए। दोनों स्त्रियों के इस संघर्ष और दृढ़ता की कहानी कहता है विद्या का डॉक्टर बन जाना।
विद्या और अमोल आम्टे आज की पीढ़ी का प्रतिनिधि चरित्र हैं, जबकि विद्या की मां रहन-सहन से पारंपरिक होते हुए विचारों से आधुनिक महिला की प्रतिनिधि पात्र।
पत्रकारों की नादानी
फिल्म पा दिखलाती है कि आम्टे समझदार और ईमानदार युवा एमपी है। किसी करप्शन का वह साझीदार नहीं। वह समाज के वंचित वर्ग के लिए काम करना चाहता है, पर दलाल मार्का नेता राह का रोड़ा बनते हैं। इस कड़ी में कुछ पत्रकार भी हैं, जो अपनी नासमझी और नादानी से इस रोड़े को चट्टान में तब्दील करते हैं। वह ब्रेकिंग न्यूज की हड़बड़ी में कैसे न्यूज का मर्म तोड़ते करते हैं। सेंसेशनल बनाने के चक्कर में न्यूज को डिफरेंट शेप और सेंस देते हैं। अपनी सतही जानकारी और अधकचरी सूचनाओं से दर्शकों और पाठकों को गुमराह करने वाले पत्रकारों को आईना दिखाती है यह फिल्म।
आम्टे का पश्चाताप
फिल्म जब अंत के करीब पहुंचती है, तो अमोल आम्टे को पता चलता है कि औरो उसका बेटा है। हालांकि दोनों की मुलाकात से ही फिल्म शुरु हुई है। आम्टे एमपी बन चुका है। पर तब आम्टे के लिए औरो महज एक ऐसा बच्चा है जिसे प्रोजेरिया ने जकड़ रखा है। आम्टे के भीतर उस असामान्य बच्चे के लिए सिम्पैथी के भाव हैं। वह उसकी हर मुराद पूरी करना चाहता है। इसी क्रम में कई बार वह उसके नाज-नखरे भी सहता है। वैसे तो हर बच्चे का मन बहुत कोमल होता है, पर किसी बीमार बच्चे का मन हर किसी को कुछ ज्यादा ही कोमल लगने लगता है। ऐसा ही होता है आम्टे के साथ भी। उसके मन में औरो के लिए खास जगह बन जाती है। ऐसे में जब उसे पता चलता है कि औरो का वक्त अब खत्म होने वाला है, तो बेचैन सा वह भागा चला आता है उस हॉस्पिटल में जहां औरो एडमिट है। औरो के वॉर्ड में पहुंचते ही उसकी मुलाकात विद्या से होती है और आम्टे को पता चलता है कि औरो उसका बेटा है।
एमपी बन चुके आम्टे को अपनी चूक का अहसास होता है। जिसे उसने कभी लिजलिजी संवेदना समझा था, आज उस संवेदना को महसूस कर रोमांच से भर रहा है। इस बीच आम्टे और औरो के रिश्ते की बात उसके विरोधियों और मीडिया तक भी पहुंच जाती है। सब इसे अपने तरीके से भुनाने में जुट जाते हैं। पर आम्टे बगैर किसी लाग लपेट के इस सच को स्वीकार करता है। वह स्वीकार करता है कि उसने एक नाजुक मोड़ पर जो फैसला किया था, वह गलत था और अब वह अपनी गलती को सुधारना चाहता है।
फिल्म का यह दृश्य अपने संदेश की वजह से बहुत मजबूत बन पड़ा है। किसी भी चूक की आत्मस्वीकृति के लिए बड़ी हिम्मत की जरूरत होती है। क्या वाकई यह हिम्मत हममें है?
औरो के पीछे भागती एक छोटी बच्ची
पूरी फिल्म में साथ के लिए औरो के पीछे भाग रही एक बच्ची दर्शकों का ध्यान अपनी ओर बार-बार खींचती है। फिल्म हॉल में बैठे दर्शकों को कभी यह बात गुदगुदाती है तो कभी मंद मुस्कान से घेर लेती है। पर फिल्म जब अपने अंत के करीब पहुंचती है तो पूरी फिल्म में बिना संवाद के मौजूद इस लड़की की उपस्थिति की सार्थकता नजर आती है। वह हॉस्पिटल में आई है बीमार औरो से मिलने। उसके हाथ में एक कागज है। वही कागज जो वह ऑरो को इससे पहले भी देना चाहती थी, मगर औरो के भाग जाने के कारण कभी दे न पाई। इस कागज में एक स्केच बना है। यह औरो की ही तस्वीर है। पर इसमें लकीरें नहीं हैं। पूरा स्केच तैयार है सॉरी के रोमन लेटर से। वह कहती है कि वह वाकई डर गई थी पहली बार औरो को देख कर। अनजाने में उसने औरो का उपहास उड़ाया था। पर उसने उस भूल को स्वीकारने की कई बार कोशिश की, पर औरो ने उसे यह वक्त कभी नहीं दिया। वह कहती है कि जीवन में जब कोई गलती हो जाए, तो उससे दूसरों को तो दुख होता ही है, पर गलती करने वाले को जब अपनी गलती का अहसास होता है तो उसे सामने वाले शख्स से ज्यादा पीड़ा होती है।
जीवन में अगर हम भी इसी तरह चीजों को समझने लगें तो कई ऐसे रिश्ते जो टूट चुके हैं, जुड़ते नजर आएंगे।
और अब औरो की बात
औरो। बारह साल का बच्चा। प्रोजेरिया से पीड़ित। बेहद संवेदनशील। बिल्कुल अपनी मां और नानी की तरह। स्कूल के बच्चों के बीच उसकी खास पहचान। अपनी थकान से कई बार हतप्रभ सा। कई बार क्षुब्ध सा। पर ऐसा नहीं कि उसका क्षोभ दूसरों पर उतार दे। उसे पता है कि उसे मसालेदार चीजें नहीं खानी। वह नहीं खाता। खिचड़ी खा कर संतोष कर लेता है। उसे मां ने बता दिया है कि उसका पिता एमपी अमोल आम्टे है। उसे यह भी पता है कि आम्टे को उसका ही राज नहीं पता। वह कई बार आम्टे से मिलता है, पर उसे नहीं बताता है। एकाध दफे बताने को होता है फिर अपनी ही बात को बालसुलभ चंचलता से ढंक लेता है। चंचलता के इस आवरण में छुपी उसकी गंभीरता दर्शकों को लुभाती है।
निर्देशन में खटकने वाली एक बात
औरो बहुत नाजुक है। इतना नाजुक कि वह पत्थरों पर बैठ नहीं सकता। क्रिकेट के मैदान में थोड़ा दौड़ जाये तो हॉस्पिटल पहुंच जाता है। पर वही औरो जब फील्ड में या मेट्रो ट्रेन में मंकी डांस करता है, तो उसका शरीर न तो थकता है, न उसे किसी सहारे की जरूरत पड़ती है। इन दो दृश्यों में औरों का शरीर अलग-अलग तरीके से बिहेव करता है। लगता है बाल्की यहां पर मंकी डांस करवाने के लोभ का संवरण नहीं कर पाये।