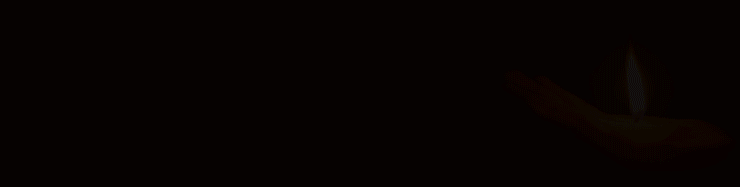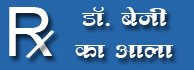भाषा की गति लोक व्यवहार से तय होती है। इसी के आधार पर मानक बनते हैं और तब तैयार होता है उसका व्याकरण। ठीक ऐसी ही बात परंपरा के लिए भी कही जा सकती है। बदलते वक्त के साथ परंपराएं भी बदलती हैं और उनका व्याकरण भी। तो बदल रही परंपराओं और बन रहीं मान्यताओं की ओर इशारा करता संजय खाती का यह नजरिया पेश है आपके लिए :
---------------------------------------------------------------
गुजरा हफ्ता हमारे लिए बेहद तकलीफदेह रहा। नोएडा में आरुषि मर्डर केस खबरों पर छाया रहा, जिसमें तमाम अटकलों के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि चौदह साल की इस प्यारी सी बच्ची की हत्या उसके पिता ने की। उधर मुंबई में एक प्रेमी-प्रेमिका ने मिलकर एक युवक का बेदर्दी से कत्ल कर दिया। ये दोनों केस पुलिस के दावे पर आधारित हैं और जैसा कि आप जानते हैं, पुलिस के दावों को भी अदालत में सही साबित करना होता है और तभी इस बात का फैसला होता है कि कसूरवार कौन था। लेकिन फिलहाल जो डिटेल्स सामने आए हैं, वे आम नागरिक का दिल दहला देने वाले हैं और जाहिर है, यह सवाल उठे बिना नहीं रहता कि हमारे समाज को क्या हो गया है?
इस नतीजे पर पहुंचना बेहद आसान है कि हमारे समाज का नैतिक पतन हो रहा है। मीडिया ने जिन एक्सपर्ट्स से बात की है, उनकी भी राय यही है कि सोशल वैल्यू सिस्टम में गिरावट आ रही है, समाज का नैतिक तानाबाना बिखर रहा है, क्योंकि लोग स्वार्थी होते जा रहे हैं। वे अपनी सुख-सुविधा के आगे किसी चीज की कीमत नहीं समझते, लिहाजा हर तरह के अपराध बढ़ रहे हैं, यहां तक कि पवित्र रिश्तों की इज्जत भी बची नहीं रही।
है, उनकी भी राय यही है कि सोशल वैल्यू सिस्टम में गिरावट आ रही है, समाज का नैतिक तानाबाना बिखर रहा है, क्योंकि लोग स्वार्थी होते जा रहे हैं। वे अपनी सुख-सुविधा के आगे किसी चीज की कीमत नहीं समझते, लिहाजा हर तरह के अपराध बढ़ रहे हैं, यहां तक कि पवित्र रिश्तों की इज्जत भी बची नहीं रही।
 है, उनकी भी राय यही है कि सोशल वैल्यू सिस्टम में गिरावट आ रही है, समाज का नैतिक तानाबाना बिखर रहा है, क्योंकि लोग स्वार्थी होते जा रहे हैं। वे अपनी सुख-सुविधा के आगे किसी चीज की कीमत नहीं समझते, लिहाजा हर तरह के अपराध बढ़ रहे हैं, यहां तक कि पवित्र रिश्तों की इज्जत भी बची नहीं रही।
है, उनकी भी राय यही है कि सोशल वैल्यू सिस्टम में गिरावट आ रही है, समाज का नैतिक तानाबाना बिखर रहा है, क्योंकि लोग स्वार्थी होते जा रहे हैं। वे अपनी सुख-सुविधा के आगे किसी चीज की कीमत नहीं समझते, लिहाजा हर तरह के अपराध बढ़ रहे हैं, यहां तक कि पवित्र रिश्तों की इज्जत भी बची नहीं रही। मेरा मानना है कि यह एक आसान जवाब है, और जैसा कि होता है, आसान जवाब सही जवाब नहीं होते। वे हमें इसलिए पसंद आते हैं कि हमें ज्यादा सिर खपाने से फुर्सत मिल जाती है। यह सही है कि पुराना वैल्यू सिस्टम बिखर रहा है, लेकिन सिर्फ इतने से ही जुर्म बढ़ने का दावा साबित नहीं हो जाता। सबसे पहले तो यह बात ही बहस में है कि जुर्म बढ़ रहे हैं।
हमारे पास जो आंकड़े हो सकते हैं, वे काफी नए हैं। मसलन हम यह पता नहीं लगा सकते कि बीस, पचास या सौ साल पहले अपराध कम होते थे या ज्यादा। इसकी वजह रिपोर्टिंग सिस्टम है। आज का समाज कहीं ज्यादा संगठित है, लोग ज्यादा जागरूक हैं और सिस्टम ज्यादा कारगर है, इसलिए अनगिनत ऐसे केस भी अब दर्ज होने लगे हैं, जो पहले नहीं हो पाते थे।
मुझे लगता है कि जुर्म तब भी होते थे और बड़ी तादाद में होते थे, लेकिन वे पुलिस केस नहीं बनते थे। जिन मामलों को आज हम वैल्यू सिस्टम टूटने की मिसाल मानते हैं, वे भी हर युग में हुए हैं। इतिहास और पुराणों को देखिए, जहां राजपाट के लिए भाइयों और पिता की हत्या के किस्से आम हैं, बल्कि जायज ठहराए गए हैं। परिवार के भीतर बदकारी (इंसेस्ट) के आरोप से तो देवता भी बरी नहीं हैं।
परिवार और समाज का विकास होने के बाद भी उनकी नैतिकता को लगातार चैलेंज किया जाता रहा है। पिछड़े समाजों में ऐसे-ऐसे अत्याचार होते हैं कि रूह कांप जाए। पाकिस्तान के कबाइली इलाकों में किसी कुनबे को सजा देने के लिए उस कुनबे की महिला से सामूहिक बलात्कार का मामला हाल में इंटरनैशनल मुद्दा बन गया था, जब मुख्तारन माई ने बगावत कर दी थी।
जिन्हें क्राइम ऑफ पैशन कहा जाता है, यानी जज्बाती अपराध जैसे कि नोएडा और मुंबई के केस हो सकते हैं, उनकी भी कमी कभी नहीं रही। शहरों से दूर ऐसे किस्से सैकड़ों मिल जाएंगे, जिन्हें इज्जत के नाम पर दबा दिया जाता है।
यहां तक कि शहरों में भी ऐसे केस हमेशा होते आए हैं। फर्क यह है कि वे हाई प्रोफाइल केस नहीं होते। ज्यादा से ज्यादा वे पुलिस फाइलों में गुम हो जाते हैं, मीडिया उन्हें तवज्जो नहीं देता। लेकिन जब उसे कोई हाई प्रोफाइल सनसनीखेज मामला मिल जाता है, तो उसके शोर की इंतहा नहीं रहती। इस शोर का असर हम पर जबर्दस्त होता है और हम डिप्रेशन के शिकार हुए बिना नहीं रहते। हमें लगने लगता है कि दुनिया ने अपनी धुरी पर घूमना छोड़ दिया है। हम नरक में जा रहे हैं। सब कुछ खत्म हो रहा है।
यह एक बुजुर्ग सोच है। हर उम्रदराज शख्स को लगता है कि उसका जमाना बेहतर था और अब अच्छाई खत्म होती जा रही है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ जीवन का जोश धीमा पड़ने लगता है, थकान और ऊब के धुंधलके के पार नए जमाने की हलचलें भुतहा दिखने लगती हैं। हर पुरानी पीढ़ी को नई पीढ़ी उद्दंड, बदतमीज और बेसब्र नजर आती है।
वक्त की करवटें गुजरे जमाने की शरारतों को इतना मासूम बना देती हैं कि उनके बरक्स मौजूदा दौर हाहाकारी लगने लगता है। लेकिन सच तो यही है कि हर नया जमाना पहले से ज्यादा बिंदास, तरक्कीपसंद, शौकीन और मेहनती साबित होता है। इसीलिए समाज आगे बढ़ता है, वह कभी जंगलों की ओर नहीं लौटता।
तो समाज के पतन की थ्योरी को गलत मानते हुए मैं दो नतीजों तक पहुंचना पसंद करूंगा। एक तो यह कि समाज नीचे नहीं जा रहा, वह अपने रास्ते पर है, जैसी कि उसकी फितरत है, और दूसरा, नैतिकता की जिस गिरावट का रोना हम रोते रहते हैं, वह असल में नैतिकता के मतलब बदल जाने से पैदा हुई गलतफहमी और तानव का मामला है।
इस दूसरे मुद्दे का थोड़ा सा खुलासा शायद जरूरी है। नए जमाने में पुराने पैमाने टूट रहे हैं, जैसे कि विवाह और परिवार की संस्थाएं। जाहिर है, इसके साथ रिश्तों के मायने भी बदलेंगे। लेकिन इसमें वक्त लगता है। भारत जैसे समाज में, जहां परंपरा काफी मजबूत रही है, यह काम और भी मुश्किल होगा। लिहाजा पुराने मूल्यों को बचाने की जिद भी होगी, नए का लालच भी और डर भी।
विवाह से पहले और विवाहेतर रिश्ते आम बात होते जा रहे हैं, लेकिन उनके साथ जुड़ी उलझनें भी। अगर हम पुलिस के दावे को मानें, तो आरुषि के मर्डर जैसा केस अमेरिकी समाज में नहीं घट सकता, जबकि भारत में उसके पूरे चांस हैं। पश्चिम में परिवार की थीम इतनी कमजोर पड़ चुकी है कि पिता को अपना रिश्ता छिपाने और इज्जत बचाने के लिए इस हद तक जाने की जरूरत नहीं होती। उसे बेटी के किसी रिश्ते पर भी नाराज होने का हक नहीं होता।
इसी तरह मुंबई वाले मामले का निपटारा भी वहां दूसरे तरीके से हो सकता था। अलबत्ता उस केस से जुड़ी बेरहमी जरूर चौंकाने वाली बात है, लेकिन ऐसा पागलपन कब नहीं था? क्राइम ऑफ पैशन हर जमाने और हर समाज में होते रहेंगे। इंसान सृष्टि का सबसे अक्लमंद जीव है। उसके गिरने की कोई हद नहीं है, लेकिन आखिरकार अपनी सामूहिकता में वह ऊपर ही उठता देखा गया है। दिन-रात हमें घेरे हुए इन डरावने किस्सों और तमाम अपशकुनों के बावजूद इस सचाई पर भरोसा क्यों नहीं किया जाना चाहिए?
साभार : नवभारत टाइम्स