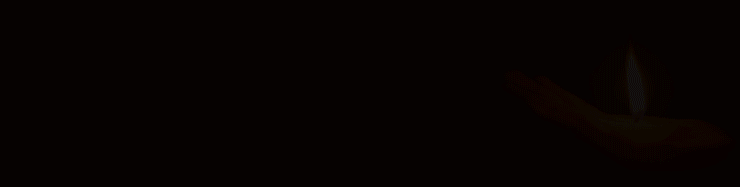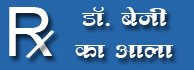प्रिय अखिल,
पहला पत्र इसलिए लिखा था कि मेरे जिंदा होने की जानकारी तुम सबों के पास हो। दूसरा पत्र लिखने की इच्छा नहीं थी। पर तुम्हारा पत्र मिलने के बाद लिखना जरूरी लगा। अपनी सफाई देने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि औरतों के बारे में सोचने का तुम्हारा तरीका बदले। साथ ही तुम यह जान सको कि तुम्हारी यह 'कलमुंही' बहन घर से क्यों भागी थी।
तब तुम सिर्फ12 साल के थे, आज 22 के हो। इन दस सालों का सच है कि

मैंने दस घाट का पानी पी लिया। 27 की हो गई, पर लगता है अनुभव मेरे पास 67 से भी ज्यादा के हो गए। तुम्हारी उम्र पर ध्यान इसलिए चला गया मेरे भाई, कि तुम्हारे पत्र में 'मर्द' की बू थी। मर्द जिसे मैंने 17 की उम्र में झेला था पहली बार।
तुमने लिखा था कि मेरे नाम की चर्चा होने से ही चाचा हत्थे से उखड़ जाते हैं; उखड़ें भी क्यों नहीं, आखिर उन्होंने ही उखाड़ा था न मुझे। अखिल, मैं याद नहीं करना चाहती उस पल को... पर बुरी तरह टूट गई थी मैं उस रोज। अब तो उन्हें चाचा कहते हुए भी उबकाई आती है।
खैर, छोड़ो उस बात को। हां, तो मैं भाग कर आ गई थी दिल्ली। हर तरफ ऊंची-ऊंची, चौड़ी-चौड़ी सड़कें, तेज भागतीं गाड़ियां; इस नए तरह के शहर को देख बदहवास हो गई थी। सड़क पार करने की कोशिश में किसी गाड़ी की चपेट में आ गई। पता नहीं किसने, कैसे और कब मुझे एम्स पहुंचा दिया। दस दिनों तक भर्ती रही। सिर में चोट लगी थी। दो दिनों तक बेहोश रही। होश में आने पर लोगों ने नाम, पता-ठिकाना पूछा। मैं चुप रही। लोगों ने समझा, याददाश्त चली गई है। पहुंचा दिया निश्छल छाया के नारी निकेतन में। साल भर रही वहां। मर्दो की छाया से भी डरती थी। धीरे-धीरे सामान्य हुई। कब तक बैठी रहती नारी निकेतन में, निकलना शुरू किया। शहर में काम और भविष्य की तलाश में कई दफ्तरों के चक्कर काटे। इस भटकाव ने आंखों को अभ्यस्त बना दिया मर्दों की घूरती निगाहों को सहने का। नौकरी मिली एक प्रकाशक के पास, किताबों की प्रूफ रीडिंग करने की। लगभग 9 साल गुजर गए यहां।
धर्म-अध्यात्म, समाज-राजनीति, संबंधों की दुनिया की किताबें चाटती रही। पढ़ती रही और खूब पढ़ी। खुद-ब-खुद विचार भी पनपते रहे। सबको संजोती हुई आज अपने को मच्योर्ड महसूस करती हूं। डरावनी छायाएं अब मेरा पीछा नहीं करतीं।

घर में भी देखती थी कि औरतों को फैसला करने की इजाज़त नहीं थी। शुरू में समझती थी कि यह स्थिति सिर्फ हमारे घर में है; लेकिन अखिल, यह तो घर-घर की कहानी है। हो भी क्यों नहीं, इस समाज में तो पुरुषों का राज चलता है न। लेकिन इस समाज में मैंने अपना फैसला किया और उस पर अमल भी। फैसले करने का अपना सुख होता है।
प्रूफ रीडिंग का काम करते हुए 'प्राचीन शिव पुराण' पढ़ने का मौका मिला। उसके उमा संहिता के चौबीसवें अध्याय में औरतों को लेकर जो टिप्पणियां हैं, उन्हें पढ़कर खून खौल जाता हैं। उसका सार संक्षेप यही है कि औरतें मंदबुद्धि और नीच होती हैं। हर पाप की जड़ में औरत है। परंपरागत शिष्टाचार की मर्यादा को नहीं निबाहतीं और वे पतियों का साथ इसलिए नहीं छोड़तीं कि उन्हें कोई दूसरा मर्द घास नहीं डालता। जानते हो, इस किताब को पूरी आस्था के साथ संभाल कर रखा था कि यह पुराण है। जबसे यह चैप्टर पढ़ा, मुझे इससे और ऐसी तमाम किताबों से घृणा हो गई।
तुम्हारे पत्र से जाना कि घर के लोगों को इस 'कलमुंही' का जिंदा रहना अखर गया। 'कलमुंही' संबोधन इसीलिए न कि मैं अकेले रहती हूं, पता नहीं कितनों से मेरे संबंध बने होंगे? अपने चाचा को कहना अखिल, जरा भी आशंकित न हों। मैं बाहर रह कर बेहद सुरक्षित हूं।
ओ भाई, मुझे बताओ कि तुम मर्दों ने ऐसी धारणा क्यों पाल ली है कि अगर कोई लड़की अकेली है तो उसे आसानी से पाया जा सकता है? क्या इसलिए कि वह 'असूर्यपश्या' वाली छवि तोड़ कर घर की दहलीज से निकली; कि तुम्हें अपना वर्चस्व टूटता नजर आ रहा है; कि नई पीढ़ी ने पुरुषों की पोशाक धारण कर ली है?

जानते हो अखिल, यहां जब मैं पहली बार टी-शर्ट और जींस पहन कर निकली, बड़ी असहज थी। सकुचाई हुई, यह सोच कर कि लोगों को हास्यास्पद लग रहा होगा। कुछ वैसा ही, जैसे मुझे हनुमान जी की कोई तस्वीर मिल जाए, जिसमें वे पतलून पहने दिख रहे हों। लेकिन बता नहीं सकती कि उस रोज बसयात्रा में कितनी सहूलियत हुई। इन वर्षों में जाना कि बड़ा से बड़ा परिवर्तन जरूरत की वजह से ही होता है। सहूलियत भी जरूरत का ही एक रूप है। शेर के नख और हरिण की टांगें उनकी जरूरत के मुताबिक ही विकसित हुए हैं। स्त्री आज अगर एक नए रूप में दिख रही है, तो यह नया रूप भी जरूरतों ने ही बनाया है। 'पढि़ए गीता और बनिए सीता' जैसी सीख अब उसके लिए बेमानी होती जा रही है। आज अगर उसके नख बढ़ गए हैं, अगर इतनी आक्रामक हो गई है, तो जाहिर है कि इस समाज में अपने अस्तित्व को बचाए रखने की उसने जरूरत समझी हो।
हो सकता है, मेरी बातें तुम्हें नागवार लगें। लेकिन भाई, मुझे बताओ; तुम मर्दों की जमात जब भी स्त्रियों की आधुनिकता और परंपरा की चर्चा करती है, तो ऐसा क्यों लगता है कि चुंबक के साउथ और नॉर्थ पोल की चर्चा हो रही है? तुम्हारी बहसों में लगता है कि परंपरा और आधुनिकता दो बिल्कुल अलग चीजें हैं, प्रकृति और रूप दोनों स्तरों पर। आधुनिकता को देखने की तुम्हारी यह दृष्टि कि यह परंपरा के खिलाफ संघर्ष है - आधुनिक नहीं है मेरे भाई। मुझे लगता है कि आधुनिकता कोई नई चीज़ नहीं, बल्कि वह तो परंपरा का एक्सटेंशन है। प्रकृति और रूप दोनों स्तरों पर परिमार्जित एक्सटेंशन।
जरा बताओ, जिस वक्त नरगिस फिल्मों में काम कर रही थीं, क्या वह उस दौर के लिए आधुनिक नहीं थीं? आधुनिकता और बोल्डनेस को जो लोग मल्लिका सेहरावत के कम कपड़ों में देखते हैं, उनके लिए यह विचारणीय होगा कि क्या ब्लू फिल्मों की नायिका को अति आधुनिक मान लिया जाए? तुम इन्हें 'मॉडर्न' ख्यालों वाली लड़की की बात कहकर शायद टाल जाने की कोशिश करो। लेकिन यह सच है कि फिल्म या जीवन में किसी नायिका के मार्फत आधुनिकता को समझने के क्रम में पुरुषों की निगाह फिसल कर उनके कम कपड़ों पर अटक जाती है, जबकि हकीकत है कि कपड़े में ही आधुनिकता नहीं होती। अगर ऐसा होता, तो मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी, कल्पना चावला को आधुनिक माना ही नहीं जाना चाहिए था।
आधुनिकता का संबंध तो दृष्टि, विचार और कृत्य से होता है। हमारी दृष्टि वक्त की नब्ज पर अपनी पकड़ रखती है, विचार हमें उसका परिमार्जित रूप दिखाते हैं और हमारे कृत्य आनेवाली पीढ़ी के लिए दृष्टि, विचार और कृत्य के लिए जगह बनाते चलते हैं। यह तो पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलने वाला सिलसिला है। इसी प्रक्रिया के तहत समाज आधुनिक होता चलता है।
एक और बात, तुम मर्दों की दुनिया हमेशा औरतों को औजार की तरह क्यों इस्तेमाल करती है? उसे साध्य बनाने की बजाय साधन क्यों बनाती है, आश्रय की जगह आलंबन क्यों? कबीर की दृष्टि धर्म, प्रेम और ईश्वर को लेकर आधुनिक और तार्किक दिखती है, लेकिन स्त्रियों के मामले में वह इतने अनुदार क्यों हैं, तुम्हारी तरह? उन्होंने ही लिखा है 'नारी की झाईं पड़त अंधा होत भुजंग। कबिरा तिनकी कौन गति, जे नित नारी संग'। एक तरफ नारी के प्रति ऐसी दृष्टि और फिर परमात्मा से संबंध बनाने के लिए उन्होंने खुद को उसकी बहुरिया (स्त्री रूप) में पेश किया। कैसी है तुम्हारे मर्दों की दुनिया रे अखिल!
देख न अखिल, पिताजी ने तेरा नाम अखिल रखा था और मेरा बिंदु। उनके लिए तू संसार था, मैं तो महज बिंदु। लेकिन आज मैं वृत्त बन गई अपने में सिमटी हुई।
घर से भागने का अफसोस सिर्फ यह है कि मेरे न होने से तू स्त्रियों के मनोभावों को समझने में अपरिपक्व रह गया; तेरी दृष्टि सामंती हो गई। बड़ी दीदी होने का कोई दायित्व मैं नहीं निभा सकी। पर पता नहीं क्यों, तुझसे इतनी उम्मीद करती हूं कि स्त्रियों का सम्मान करना सीख, चाहे वह तेरी मां हो, पत्नी, बहन या फिर पड़ोसन।
तुम्हारी दीदी
बिंदु
(प्रकाशित)
 शहरी होना बड़ी बात नहीं, शहरी का शरीफ़ होना बड़ी बात है। आप सोच रहे होंगे कि यह कैसी बेतुकी बात कर दी मैंने। शहरी और शरीफ़ शहरी में कोई अंतर होता है क्या? यक़ीनन, अंतर होता है और बहुत ही गंभीर और गहरा अंतर होता है। रूप और बनावट में दोनों दिखते एक से हैं पर शरीफ़ शहरी बड़ी शार्प चीज़ होता है। वह इतनी तेज़ छुरी होता है कि आपकी गरदन काट ले जाए और आपको दर्द तक का अहसास न होने दे। इसे आप आसानी से ऐसे समझें कि यह शरीफ़ शहरी की बातों का जादू होता है कि आप अपनी गरदान बार-बार और सहर्ष उसके सामने प्रस्तुत करते हैं कि ले भाई, काट ले जा मेरी गरदन।
शहरी होना बड़ी बात नहीं, शहरी का शरीफ़ होना बड़ी बात है। आप सोच रहे होंगे कि यह कैसी बेतुकी बात कर दी मैंने। शहरी और शरीफ़ शहरी में कोई अंतर होता है क्या? यक़ीनन, अंतर होता है और बहुत ही गंभीर और गहरा अंतर होता है। रूप और बनावट में दोनों दिखते एक से हैं पर शरीफ़ शहरी बड़ी शार्प चीज़ होता है। वह इतनी तेज़ छुरी होता है कि आपकी गरदन काट ले जाए और आपको दर्द तक का अहसास न होने दे। इसे आप आसानी से ऐसे समझें कि यह शरीफ़ शहरी की बातों का जादू होता है कि आप अपनी गरदान बार-बार और सहर्ष उसके सामने प्रस्तुत करते हैं कि ले भाई, काट ले जा मेरी गरदन। शरीफ़ शहरी होने का ठप्पा अपने ऊपर लगवा पाते हैं। इसलिए कहता हूं कि शरीफ़ शहरी बनना यक़ीनन बड़े धैर्य का काम है। वह इतना आसान नहीं कि आज आपने सोच लिया और कल से आप शरीफ़ शहरी बन गये। जो भी सज्जन फिलहाल इस टिप्पणी को पढ़ रहे हैं, उनके बारे में मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि वे शहरी तो हैं पर शरीफ़ शहरी नहीं। क्योंकि शरीफ़ शहरी पढ़ने के रोग से बिल्कुल मुक्त होता है। वह सिर्फ़ पट्टी पढ़ाना जानता है। वह किसी भी वक़्त, किसी के भी ख़िलाफ़, किसी को कोई भी पट्टी बड़ी आसानी से पढ़ा सकता है।
शरीफ़ शहरी होने का ठप्पा अपने ऊपर लगवा पाते हैं। इसलिए कहता हूं कि शरीफ़ शहरी बनना यक़ीनन बड़े धैर्य का काम है। वह इतना आसान नहीं कि आज आपने सोच लिया और कल से आप शरीफ़ शहरी बन गये। जो भी सज्जन फिलहाल इस टिप्पणी को पढ़ रहे हैं, उनके बारे में मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि वे शहरी तो हैं पर शरीफ़ शहरी नहीं। क्योंकि शरीफ़ शहरी पढ़ने के रोग से बिल्कुल मुक्त होता है। वह सिर्फ़ पट्टी पढ़ाना जानता है। वह किसी भी वक़्त, किसी के भी ख़िलाफ़, किसी को कोई भी पट्टी बड़ी आसानी से पढ़ा सकता है।  शरीफ़ शहरी की एक बड़ी खासियत यह होती है कि वह सबकी "हां" में "हां" मिलाता है। राग दरबारी पर उसका एकाधिकार होता है। गरीब की जोरू मजबूरी में सबकी भौजी हो जाती है, पर शरीफ़ शहरी जानता है कि इस भौजी से कब, कहां और कैसे मिलना है। मुहावरों की ज़बान में बात की जाए तो शरीफ़ शहरी के कई-कई मौसेरे भाई होते हैं। आपकी ज़रूरत के वक़्त वह बड़े इतमीनान से नौ दो ग्यारह हो जाता है। लेकिन कभी उसे आपकी ज़रूरत पड़े तो वह बारह दस बाइस की स्पीड से आपके पास दौड़ा चला आएगा। यानी अपना काम निकालने के लिए वह हर तरह का नौ छौ करने को तैयार रहता है। साथ ही आपके बन रहे काम को तीन तेरह करने में उसे दो मिनट भी नहीं लगते। महानगरों में शरीफ़ शहरी बनने का फैशन अपने पूरे उफान पर है। शराफ़त का यह किटाणु अब गांवों और कस्बों में भी अपनी ज़मीन तलाशने लगा है। तो तय करें आप कि आप शहरी बनना पसंद करेंगे या शरीफ़ शहरी।
शरीफ़ शहरी की एक बड़ी खासियत यह होती है कि वह सबकी "हां" में "हां" मिलाता है। राग दरबारी पर उसका एकाधिकार होता है। गरीब की जोरू मजबूरी में सबकी भौजी हो जाती है, पर शरीफ़ शहरी जानता है कि इस भौजी से कब, कहां और कैसे मिलना है। मुहावरों की ज़बान में बात की जाए तो शरीफ़ शहरी के कई-कई मौसेरे भाई होते हैं। आपकी ज़रूरत के वक़्त वह बड़े इतमीनान से नौ दो ग्यारह हो जाता है। लेकिन कभी उसे आपकी ज़रूरत पड़े तो वह बारह दस बाइस की स्पीड से आपके पास दौड़ा चला आएगा। यानी अपना काम निकालने के लिए वह हर तरह का नौ छौ करने को तैयार रहता है। साथ ही आपके बन रहे काम को तीन तेरह करने में उसे दो मिनट भी नहीं लगते। महानगरों में शरीफ़ शहरी बनने का फैशन अपने पूरे उफान पर है। शराफ़त का यह किटाणु अब गांवों और कस्बों में भी अपनी ज़मीन तलाशने लगा है। तो तय करें आप कि आप शहरी बनना पसंद करेंगे या शरीफ़ शहरी।